द्रवेषु चिर कालस्थं द्रव्यं यत्सन्धितं भवेत।
आसवारिष्ट भेदेस्तु प्रोच्यते भेषजो चितम् ।।
अर्थात् जल, क्वाथ, स्वरस आदि पतले पदार्थों में गुड़, चीनी, मधु आदि घोलकर-छायाफूल, बबूल छाल, महुआ (मधूक-पुष्प) आदि मिलाकर सन्धान करके रखने पर उनमें जो वस्तु चिरकाली स्थायी (बहुत समय तक रखने पर भी नष्ट न होने वाली) उत्पन्न होती है-यह ओषधोपयोगी है तथा उसके आसव-अरिष्ट (Aasva-Arishta)आदि कई भेद (प्रकार) कहे जाते हैं।
* वनस्पतियों के स्वरस, कषाय (काढ़े) आदि द्रव पदार्थ बनाकर वैसे ही पड़े रखने पर, कुछ दिनों के बाद दोषपूर्ण हो जाते हैं। अतः वे स्थायी गुणदायक बने रहे। इसीलिए “आसव-अरिष्ट”(Aasva-Arishta) का निर्माण किया गया है।
* जल में ओषधि-द्रव्य व मीठा और धाय के फूल, बबूल छाल महुआ फूहरा आदि मिलाकर कुछ दिनों तक पात्रों में रखकर जो सन्धान किया जाता है. उसे “आसव” और “अरिष्ट” कहते हैं।
~आसव(Aasva)- अरिष्ट(Arishta) मे भेद/अंतर-
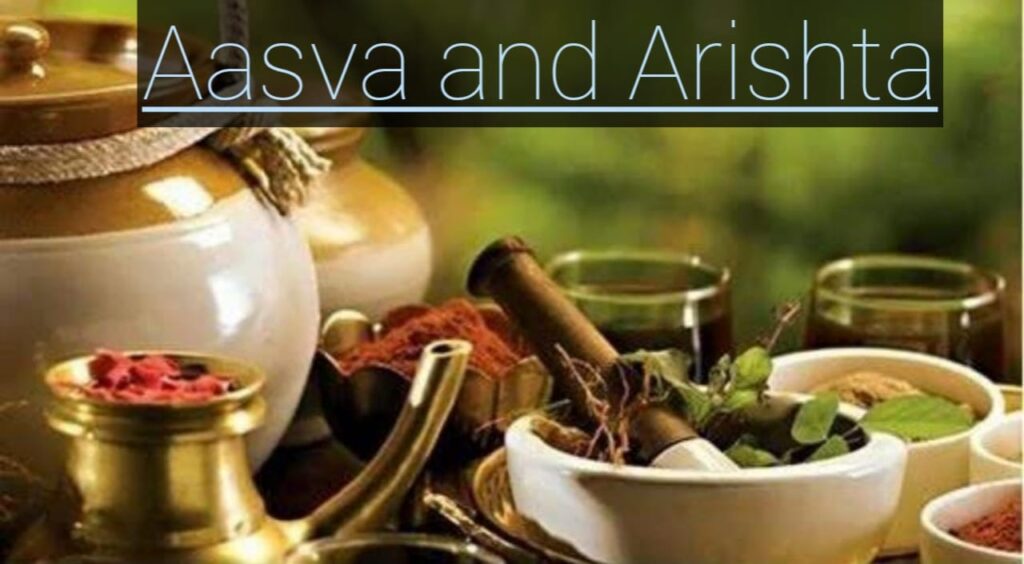
* बिना क्वाथ बनाये हुए ही कच्चे जल में ओषधी और गुड़, चीनी व मधु आदि मीठे पदार्थ और धाय के फूल, महुआ फूल, बबूल की छाल, आदि डालकर जो सन्धान किया जाता है, उसे “आसव”Aasva कहा जाता है, तथा ओषधियों का क्वाथ (काढ़ा) करके उसमें यह चीजें मिलाकर जो ओषधि तैयार की जाती है, उसे “अरिष्ट”Arishta कहते है।
परन्तु यहाँ यह बात सर्वथा यथार्थ प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि आसव नाम रहने पर भी क्वाथ करके बनाना तथा अरिष्ट(Arishta) नाम रहने पर भी क्वाथ करके न बनाने का निर्देश प्राचीनतम् और अर्वा चीनी अनेक ग्रन्थों में पाया जाता है- जैसे द्राक्षास व लोध्रासव आदि का क्वाथ करके बनाना और पिप्पल्यारिष्ट, मण्डूराद्यरिष्ट, त्रिफलारिष्ट आदि का क्वाथ न करके बनाने का विधान प्रत्यक्ष है।
~ वनस्पतियों की विशुद्धता-
आसव-अरिष्ट बनाते समय सर्वप्रथम उनके मूल द्रव्यों की ओर ध्यान दिया जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि प्रायः पन्सारी लोग बाजार में असली द्रव्यों के स्थान पर नकली द्रव्य भी बेचा करते है, जैसे- अनन्त मूल, नेत्रबाला, सफेद मूसली, रास्ना, काला जीरा, चव्य, अतीस, दाल चीनी, मुसब्बर/एलुआ, कबावचीची, चिरायता, अशोक छाल, सफेद चन्दन, दशमूल के ओषधद्रव्य, गजपीपल, कूठ, मधु, कस्तूरी तथा केसर आदि प्रायः नकली बिक्री कर देते है।
अतः इन ओषधद्रव्यों को खरीदते/क्रय करते समय पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा इन नकली ओषध द्रव्यों द्वारा निर्मित आसव-अरिष्ट ही क्या कोई भी निर्मित की जाने वाली ओषधि गुणकारी नहीं हो सकती है। कुछ चीजें मिलने पर भी उनमें कुछ अंश में मिलावट रहती है, जैसे धनिया, अजवायन, सौंफ, कालाव सफेद जीरा तथा धाय के फूल आदि। अतः इनको खूब साफ-स्वच्छ करके ही काम में लेना चाहिए।
असली व नकली (दोनों) जिसमें मिली हों, उनमें से असली को अलग करके उपयोग में लेना सम्भव हो तब तो लेना चाहिए। अन्यथा उसको छोड़ देना ही उत्तम रहता है।
~ कोई भी ओषधि-कार्य में लेने से पहले भली प्रकार साफ-स्वच्छ कर लेनी चाहिए तथा तौलते समय इस बात का ध्यान रखा जाना भी आवश्यक है कि काँटे/तराजू पर नमक, खटाई, नीबू रस आदि न लगा हुआ हो। इसी प्रकार इमाम दस्ता अथवा डिसेण्टीग्रेटर आदि को भी (जिसमें आसव-अरिष्ट के ओषधि द्रव्यों को कूटा-पीसा जाना है) भली प्रकार साफ-स्वच्छ कर लेना चाहिए, उस पर नमक
आदि कुछ भी लगा न हो तभी ओषध द्रव्यों को कूटे-पीसे अथवा लवण अथवा अम्ल-संयोग से आसव अरिष्टों में एसिड की मात्रा उत्पन्न हो जाने कारण उनके बिगड़ जाने खराब हो जाने की सम्भावना रहती है।
~ क्वाथ बनाने के लिए पीतल या ताँबे के कलईदार अथवा स्टेनलेस स्टील या मिट्टी के पात्रों का उपयोग करना चाहिए। साधारण लौह पात्र में काढ़ा बनाने से उसका रंग काला हो जाता है। तथा उसके स्वाद में भी अन्तर पड़ जाता है। एक आसव-अरिष्ट का क्वाथ समाप्त हो जाने के बाद उपयोग में लाये हुए समस्त पात्रों को छाई/राल अथवा सोड़ा मिलाकर बिचाली या चट/टाट से अथवा चूने के पानी ते खूब खुश रगड़कर भलीप्रकार साफ-स्वच्छ कर लेना चाहिए। तदुपरान्त 2-3 बार साफ-स्वच्छ जल से धोकर उनमें दूसरा (नवीन) क्वाथ बनाना चाहिए।
सन्धान हेतु प्रायः मिट्टी के पात्र, चीनी मिट्टी के पात्र, सीमेन्ट के हौज या सागवान, साबू या शीशम काठ लकड़ी के पात्र में लिए जाते है। यद्यपि मिट्टी के पात्रों में आसव-अरिष्ट बनाने की प्राचीन प्रथा है, जो आज के परिवेश में सर्वथा उचित नहीं है। क्योंकि कभी-कभी दूषित, स्वारी व नमक युक्त मिट्टी के बने पात्र में सन्धान करने से आसव-अरिष्ट खट्टे होकर खराब हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी में पात्र को गाड़ने से कभी-कभी फूटकर बह जाने का तथा पृथ्वी के ऊपर रखने से फूट जाने का और सर्दी व गर्मी की अधिकता के कारण सन्धान ठीक प्रकार से न होने का भय बना रहता है तथा बहुत सा आसवीय अंश का शोषण भी हो जाता है।
सीमेण्ट से निर्मित हौज में भी कुछ दिनों तक आसव ठीक बनते है, किन्तु उनके पुराने हो जाने पर अथवा सीमेण्ट आदि की खराबी से सन्धान क्रिया की उष्णता से सीमेण्ट गलकर आसव में घुल जाता है, जिससे आसव-अरिष्ट गाढ़े घोलयुक्त तथा गन्दे हो जाते है, वे साफ-स्वच्छ भी नहीं होते हैं तथा स्वाद में भी खराब हो जाते है, बल्कि कभी-कभी तो बोतलों में भरने पर अथवा पात्र में ही पड़े रहने पर-आसव-अरिष्ट जम कर खाक हो जाते हैं। सागवान आदि काठ/लकड़ी के पात्रों में उपरोक्त कोई दोष नहीं पायो जाते हैं।
इनमें बाहर की सर्दी-गर्मी का कोई विशेष असर प्रभाव नहीं होता है। तथा सन्धान कार्य भी ठीक प्रकार से होता है। तथा चिरकाल तक पड़े रहने पर भी वे धीरे स्वच्छ होते जाते है। अतः काठ/ लकड़ी के पात्र ही आसव-अरिष्ट निर्मित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी है, किन्तु यदि थोड़े परिमाण (मात्रा) में आसव-अरिष्ट बनाना हो तो तथा काठ/लकड़ी के पात्रों की सुविधा न हो तो यदि मिट्टी के पात्र लेना पड़े तो नीचें लिखे प्रकार के पात्र को ही उपयोग में लेना चाहिए।
~ नमक आदि रहित मिट्टी पात्र/बर्तन बनवाकर उसमें कुछ दिनों तक जल भरा रहने दें। तदुपरान्त उस पर सीमेण्ट का मोटा लेप करके बाहर से मोटे चट को लपेट दें। यदि चट के अन्दर थोड़ी रूई अथवा बिचाली काटकर भर देना और भी उत्तम रहता है। भांड के भीतर राल अथवा चपड़ा को स्प्रिट में गलाकर 5-7 बार लेप कर दें। जिससे सूक्ष्म छिद्र भी बन्द हो जाये। उसके बाद सन्धान करने से आसव-अरिष्ट का सन्धान ठीक होता है। काठ के पात्र बड़ी-बड़ी ओषधि निर्माण फार्मेसियों में रहते है, उनको देखकर तदनुकूल सरलतापूर्वक बनवाया जा सकता है।
~ पात्रों का रख-रखाव-
* जहाँ अधिक शीतल वायु अथवा गर्मी-लू (स्वव यानी ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवा) या प्रखर धूप आदि का प्रवेश, एवं कीड़े- मकौड़े व मच्छर, गन्दगी और अम्लीय पदार्थ न हो, ऐसे साफ-स्वच्छ वातावरण और साधारण वायु प्रवेश वाले स्थानों में ही पात्रों के रख-रखाव की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि अधिक गर्मी से आसवीय कीटाणुओं के कीटाणुओं के नष्ट हो जाने तथा अधिक गर्मी शीतलता के कारण खमीर न उठने के कारण आसव-अरिष्ट ठीक प्रकार तैयार नहीं होते हैं।
इसलिए अधिक कड़ी धूप, अधिक गर्मी, अधिक सर्दी एवं बरसाती हवाओं से पात्रों को सुरक्षित रखना चाहिए। पात्रों को रखने वाले स्थान को साफ-स्वच्छ रखना तथा उस स्थान पर धूप आदि देना चाहिए। काठ/लकड़ी के पात्रों को जमीन से 2-3 फुट ऊँचे स्थान पर अथवा स्टैण्ड पर रखना चाहिए, ताकि नीचे के स्थान की साफ-सफाई करने में कठिनाई न हो।
~ काष्ठ आदि बनौषधियों को जौ-कुट कर यानी मोटा-मोटा दरदरा कूटकर ही लेना चाहिए, बनौषधियों का बहुत बारीक (सूक्ष्म) चूर्ण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आसव-अरिष्ट घोल गाढ़े जैसे बन जाते है, जिससे वे जल्द साफ नहीं होते हैं। बनौषधियों को पीसने का कार्य डिसेण्टीग्रेटर मशीन से अतिशीघ्र और ठीक प्रकार से होता है। बहुत से ओषधि द्रव्य ऐसे होते हैं, जिनको मात्र साफ कर लेना ही उत्तम रहता है, जैसे-नागकेशर, अजवायन, सौंफ, नीलोफर, खस, ब्राह्मी, तालसपत्र, शंखपुष्पी, जटामांसी, पटोलपत्र, गोरखमुण्डी व शहतरा आदि धान के फूल आदि मधूक पुष्प यानी महुआ को सर्वथा साफ करके ही कार्य में लेना चाहिए।
~ जल व जल की मात्रा –
ओषधीय कार्यों में जल लेते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जल खारा, गन्दा, कीटाणु युक्त तथा अम्लीय पदार्थ मिश्रित न हों, क्योंकि ऐसे जल में आसवारिष्ट न बन कर सिरका बन जाता है। अतः साफ- स्वच्छ और ठीक स्वादयुक्त जल ही काम में लेना चाहिए। क्वाथ कर लेने पर जल का पाक स्वतः ही हो जाता है, किन्तु जिसका क्वाथ नहीं बनाते हैं, ऐसे आसवों में भी ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में जल को गर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि जल को गर्म कर लेने से जल के दूषित कीटाणुओं का नाश हो जाता है तथा सन्धान क्रिया भी अच्छी होती है।
सर्दी के मौसम में ठण्डे जल से सन्धान में विलम्ब होता है, यहाँ तक कि शीत ऋतु में कभी-कभी सन्धान क्रिया उत्पन्न ही नहीं होती है तथा मीठा व जल अथवा क्वाथ जैसे का तैसा ही पड़ा रहता है। कालान्तर में उनमें उष्णता उत्पन्न होने से पुनः सन्धान क्रिया उत्पन्न होती है, जिससे यदि बोतलों में भरा रहता है तो बोतल फूट जाती है और पात्र में रहता है।
प्रायः क्वाथ द्रव्य से चतुर्गुण, अष्टगुण या आवश्यकतानुसार इससे कम या अधिक जल देकर पकाकर अवशिष्ट जल रहने पर मीठा आदि मिलाकर सन्धान कार्य किया जाता है यह प्राचीन पद्धति है, परन्तु अब अनुभवों से यह जाना गया है कि इस प्रकार से बनाये गये समस्त आसव-अरिष्ट पूर्ण गुण युक्त नहीं होते है। (इसका कारण यह है कि क्वाथ द्रव्य में बहुत सी उड़नशील गुणयुक्त ओषधियाँ रहती है, इनका पाक करने पर बहुत सा अंश उड़ जाता है,
जैसे-अजवायन, लवंग, जीरा, सफेद चन्दन, देवदारू, सौंफ व खस आदि।) अतः जिसमें ऐसे ओषध द्रव्य हों, विशेषकर उन्हें तथा जिसमें यह द्रव्य न हों, उन्हें भी नीचे लिखे प्रकार से बनाने में आसव-अरिष्ट विशेष गुण युक्त तैयार होते है।
क्वाथ द्रव्य को (जिसमें काष्ठादिक शुष्क वस्तुएँ अधिक हों, उन्हें चतुर्गुण व मृदु और सरस ओषधियुक्त क्वाथ द्रव्य वाली ओषधि से द्विगुण गर्म जल लेकर किसी कलईदार पात्र में भिगोकर रख लें। 28 घण्टे के बाद खूब मसलकर छान लें और शेष बचे हुए क्वाथ द्रव्य में त्रिगुण अथवा चतुर्गुण जल देकर मन्दी आग पर एकाकर उचित अवशिष्ट जल रहने के उपरान्त छान लें तथा पहले का बिना पका हुआ जल भी मिलाकर पूरा कर लें और नीचे की गाद छोड़ देनी चाहिए।
तदुपरान्त उसमें पुराना गुड़, चीनी, मधु आदि मीठा और धायफूल, बबूलछाल, महुआ आदि मिलाकर प्रक्षेप देकर सन्धान करें। इस प्रकार से बनाये गये अरिष्ट पूर्ण गुणकारी व स्वादयुक्त होते हैं। (यह प्रक्रिया अरिष्ट बनाने के लिए है, क्योंकि आसव में तो स्वतः सम्पूर्ण द्रव्य महीना भर पड़े रहने से उसका सार तत्व सर्वांश में आ जाता है।
~मीठा मिश्रण करना व मात्रा(परिणाम)-
मधू (शहद), गुड़, चीनी में 3 चीजें आसव-अरिष्ट के घटक हैं। यदि इनमें खट्टापन, खारापन, गन्दापन आदि दोष हुए तो उनके द्वारा निर्मित आसव-अरिष्ट युक्त होकर तैयार होगें, उनका सेवन आयुर्वेदशास्त्र के विरूद्ध है। अतः खूब मधुर, साफ व स्वच्छ मीठा ही उपयोग में लेना चाहिए। बाजार में बिकने वाला मधु प्रायः मिलावटी/दोषपूर्ण रहता है। अतः यदि मधु (शहद) लेना हो तो खूब विश्वास पात्र व्यक्ति द्वारा निकाला हुआ ही लेना चाहिए। यदि ऐसा सम्भव न हो तो मधु के स्थान पर पुराना गुड़ ही लेना श्रेयस्कर है|
आयुर्वेद शास्त्र के पुरातन ग्रन्थों में आसव हेतु जल और मीठा ठीक-ठीक तो किसी-किसी योग में कम अथवा अधिक लिखा मिलता है। तद्नुसार बनाने से कोई आसव-अरिष्ट तो ठीक बनता है तो कोई अधिक मीठा और कोई बिल्कुल कम मीठा (फींका) होता है। मीठा कम होना या अधिक होना दोनों ही आसव-अरिष्ट के गुण में बाधक है।
अतः यदि जल कम है तो उसे द्रव द्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार बढ़ा देना चाहिए और यदि मीठा कम हो तो जल का lèk2 (आधा) भाग कर देना चहिए। उदाहरणार्थ, अश्व गन्धारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, अरविन्दा सव, पत्रांगा सव को ही में। इनमें यदि जल और मीठा का परिमाण शास्त्रानुसार दिया जाये तो कोई बिल्कुल गाढ़ा, कोई मीठा और कोई खट्टा तैयार होता है।)
क्वाथ बनाने के बाद तत्काल ही मीठा मिलाना चाहिए तथा उसे चट अथवा कपड़े से छान कर ही पात्र में डालना ही घीठा क्योंकि गुड़ आदि चीजों में कंकड-पत्थर, कीड़े/चीटियाँ बहुत सी दूषित चाहि मिली रहती है, छानने से वे सब दूर हो जाती है।) मीठा भी सब एक साध्य ची िमलाकर, जितना मीठा देना अभीष्ट/ठीक हो उसका 3 भाग पहले मिलाकर चामिल करना चाहिए। शेष भाग सन्धान समाप्ति के बाद अथवा छानने के बाद मिलाना चाहिए।
ऐसा करने से आसवों में मधुरता ठीक बनी रहती है तथा बिगड़ने का भी भय नहीं रहता है। एक साथ मीठा मिलाने से आसव गाढ़ा होकर सन्धान क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है।
~प्रक्षेप आदि मिलाने की विधि-
सन्धान समाप्ति (खमीर उठना बन्द हो जाने) के बाद एक प्रकार का मैल आसवारिष्टों के ऊपर जमा रहता है। उसको हटाकर आसवों को छानकर बाद में प्रक्षेप आदि द्रव्य कुछ लोग मिलाते है, कुछ लोग मीठा मिलाने के बाद तत्काल प्रक्षेप मिलाते है। लेखक ने स्वयं दोनों प्रकार से बनाया है और नतीजे पर पहुंचा है कि मीठा मिलाने के कुछ समय बाद ही प्रक्षेप द्रव्य डालना चाहिए। ऐसा करने से तथा निरन्तर चलाते रहने पर सन्धान समाप्ति तक समस्त प्रक्षेप धीरे-धीरे नीचे बैठ जाता है, जिससे उसका पूरा अंश आसवों में आ जाता है।
बिना 5-6 दिनों तक बिना चलाये प्रक्षेप द्रव्य जल में भली प्रकार भीगता नहीं है। अतः प्रक्षेप डालने के उपरान्त आसव-अरिष्ट को कुछ दिन तक चलाते रहना चाहिए। यदि सन्धानोपरान्त 5-6 दिन प्रक्षेप-द्रव्य मिलाने के लिए पात्र का मुँह खुला रखकर चलाया जाये जो मद्यांश बहुत कुछ अंश में उड़ता रहता है और तुरन्त प्रक्षेप मिलाकर बन्द करने से प्रक्षेप सूखा रह जाने से पूरा गुण नहीं आता है। अतः मीठा मिलाने के बाद सन्धान क्रिया चालू होने के बाद प्रक्षेप द्रव्य मिलाना उत्तम है।
~ सन्धान कार्य के समय आसवारिष्ट के पात्र के पास कान लगाकर सुनने से “सू-सूं” सदृश आवाज आती है तथा सन्धानित पात्र से एक प्रकार की तेज गन्ध (स्मैल) आती है (जिसको कार्बोनिक गैस) कहते है, जो वाष्प रूप में बाहर निकलती रहती है। इसके न निकलने से आसवों में विकृति आ जाती है। यदि पात्र का मुख खुला रहता है तब तो धीरे-धीरे विकार निकल जाता है और सन्धान क्रिया ठीक होती है। यदि पात्र का मुख तत्काल ही बन्द कर दिया जाये तो यह दूषित गैस बाहर न निकल कर वाष्प का द्रव रूप होकर पात्र के ढक्कन से टकराकर पुनः सन्धानित पात्र में ही गिरती है,
जिससे पूरा गद्यांश न बनकर उसमें एसिड की मात्रा उत्पन्न हो जाती है और छानने के बाद अम्लत्व-गुण विशिष्ट आसव तैयार मिलता है। कभी-कभी तो तत्काल बन्द कर देने से कार्बोनिक गैस का निस्सारण न होने के कारण साधारण पात्र अथवा मिट्टी के पात्र फूट भी जाते हैं। इसलिए सन्धान के समय पात्र के मुख को बन्द करके, उसके मुख के ऊपर साफ-स्वच्छ जालीदार कपड़ा अथवा हल्का चट बाँध देना चाहिए, जिससे छिद्रों द्वारा-दूषित वायु भी निकल जाती है और पात्र में किसी जीव-जन्तु आदि के गिरने का डर भी नहीं रहता है|
सन्धान समाप्ति के तत्काल बाद पात्र का मुख कपड़ मिट्टी करके बन्द कर देना चाहिए। सन्धान समाप्ति हुआ है अथवा नहीं, यह तो नित्य प्रति चलाकर देखने से भी मालूम हो जाता है। लेकिन कभी-कभी अधिक ठण्डा आदि के कारण खमीर धीरे-धीरे उठता है जो सू-सू की आवाज से साफ-साफ पता नहीं चलता है।
ऐसी दशा में दिया सलाई या तेल की बत्ती आदि जलाकर पात्र के भीतर ले जाये। यदि अमीर उठना बन्द न हुआ होगा तो दिया सलाई आदि बुझ जायेगी, किन्तु सन्धान क्रिया समाप्त हो जाने पर नहीं बुझेगी। उस समय पात्र को खुला न रखें, अन्यथा मद्यांश (एल्कोहल) उड़ जाने का भय रहता है। उसी समय ढक्कन लगाकर पात्र के मुख को कपड मिट्टी करके बन्द कर देना चाहिए।
~ जिस पात्र में आसव-सन्धान किया जाये अथवा छान रखा जाये तो. वह पात्र लबालब भरा हुआ नहीं रखना चाहिए। पात्र का 3 भाग ओषधि से पूर्ण और एक भाग खाली रखना चाहिए। विशेषकर सन्धान वाले पात्र को तो अवश्य ही खाली रखना चाहिए। (क्योंकि प्रक्षेप आदि द्रव्य फूलने से पात्र के खाली न रहने पर फट जाने अथवा उफान आकर बह जाने का भय बना रहता है।) छने हुए आसवों के रखने वाले पात्र भी यदि कुछ खाली न रखें जाये तो-मद्यांश (अल्कोहल) के उड़ने का भय रहता है। सन्धान के बाद व छानने के बाद पात्र के मुख को खूब भली प्रकार कपड़ मिट्टी करके बन्द कर देना चाहिए, ताकि आसवीय अंश उड़ने का भय न रहे।
~ आसव(Aasva) को छानना-
सन्धान समाप्ति के उपरान्त 10-15 दिनों के बाद आसों को छानकर प्रक्षेप आदि (कूड़ा) द्रव्य बाहर फेंक देना चाहिए। छानते समय पात्र के अधोभाग में स्थित गाढ़ा घोल जैसा गन्दा भाग (जाल) को हटा देना चाहिए। क्योंकि उसको मिलाने से समस्त आसव गन्दा हो जाता है और उसमें आसवीय मद्यांश भाग भी बहुत थोड़ा रहता है। आसवों को बन्द पात्र में छानना चाहिए। खुले पात्र में आसवों को छानने से वायु के लगने से कालापन दोष आ जाता है।
जितना शीघ्र हो सके आसव को छानकर पात्र को बन्द कर देना चाहिए, अन्यथा कभी-कभी उसमें वायु के प्रवेश से पुनः सन्धान क्रिया उत्पन्न हो जाती है। बिना छाने हुए पात्र से भी आसव-अरिष्ट काम में लिए जा सकते है, लेकिन यह प्रक्रिया ठीक नहीं रहती है, क्योंकि कभी-कभी सन्धान के समय कुछ असावधानी होने से मोठा भाग पात्र के तलस्थ भाग जमा एकत्रित रह जाता है और ऊपर का भाग कम मीठा रहता है|
उसमें से खर्च करने से कुछ भाग मीठा चला जाता है कुछ कम मीठा होने पर उसमें अम्लता आदि उत्पन्न हो जाने का भय अथवा छानने के बाद मीठा मिलाना हो तो बिना छाने केसे ठीक हो सकता है? अतः छानकर ही उपयोग में लाना प्रत्येक स्थिति में ठीक है। क्योंकि छानने से एक सा सम्मिश्रण हो जाता है। असवों को छानने के बाद चखकर देख लें। मिठास न हो तो आवश्यकतानुसार बीनी मिला लें। इससे आसव-अरिष्टों में मधुरता ठीक बनी रहती है तथा सुस्वाद बने रहते हैं तथा पीने में अरूचि भी नहीं होती है।
~ लौह मिश्रण-
जिसमें लौह चूरा मिलाया जाता है, उनमें साबुत लौह चूरा देने से लौहा का सर्वांग नहीं घुलता है। अतः लौह चूरा को घृत कुमारी/ग्वार पाठा के रस से भावित कर के पुट देकर भस्म बना लेना चाहिए। तदुपरान्त उस भस्म को बड़ी हरतिकी (हरड़) के क्वाथ या त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला) क्वाथ में डालकर धूप में 5-7 दिन तक रखकर चलाते रहना चाहिए। उसके उपरान्त लौह विलीन हो जाने पर आसवों में डालना चाहिए। इस प्रकार से डाला हुआ लौह का पूरा अंश आसव में आ जाता है।
~ आसवों में किण्व डालना-
जिस प्रकार दूध से दही बनाने के लिए दूध को औटाकर उसमें दही/दही का पानी, नीबू रस या खटाई आदि अम्ल पदार्थ (जामन) देकर जमाते हैं, उसी प्रकार आसव-अरिष्ट में खमीर उठाने के लिए -धातु की पुष्प, बबूल छाल, व महुआ के फूल डालते हैं। इनसे भी खमीर उठता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा सुराबीज प्रति मन आधा सेर के परिमाण में मिला दें तो सोने पर सुगन्ध हो जाता है।
किण्व के लिए जो आसव बनाने हो, उसी के (पहले के बने हुए) तलस्थ भाग को सुखाकर रख लें। यदि प्रत्येक आसव की अलग-अलग गाद सुखाना सम्भव न हो तो द्राक्षासव के नीचे की गाढ़ी गाग को सुखाकर रख लेना चाहिए और उसी को प्रत्येक आसव में डालना चाहिए। किण्व डालने से आसवों में आसवीय अंश उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं की संख्या अधिक बलवान हो जाने से अन्य एसिड उत्पन्न करने वाले कीटाणु उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, जिससे शुद्ध आसव तैयार होते हैं, जो चिरकाल तक पड़े रहने से विशेष गुणकारी बनते जाते हैं और बिगड़ने का भय भी नहीं रहता है।
~सुगंधित द्रव्य बनाना-
कस्तूरी, केशर, कर्पूर आदि को आसव-अरिष्टों के छानने के बाद जिसमें मिलाना हो तो उसी आसव अरिष्ट(Arishta) में अथवा अल्कोहल में या रेक्टीफाइड स्प्रिट अथवा स्प्रिट क्लोरोफार्म में घोट कर डालें। सन्धान के समय डालने से इनका कुछ अंश प्रक्षेप आदि में तथा कुछ गन्ध खमीर उठने के समय उत्ताप से नष्ट हो जाता है, इसलिए छानने के बाद उपरोक्त विधि से बनाकर रखे हुए आसव पात्र में या बोतलों में भरते समय मात्रानुसार डालें।
विशेष-मुनक्का, घृत कुमारी आदि किस रूप में लेना चाहिए? मुनक्का काला, आबजूस, किशमिश आदि कई प्रकार के बाजार में आते हैं। काला मुनक्का अन्य ओषधियों के लिए तो श्रेष्ठ होता है, परन्तु उसमें अम्लता रहने से आसवों के काम के योग्य नहीं होता है। किशमिश यदि मधुर हो तो काम में ली जा सकती है, परन्तु आसवों के लिए आबजूस (बड़े दाने का लाल मुनक्का) ही सर्वदा उपयुक्त होता है। बाजार में सड़े-गले रस रहित तरह-तरह के मुनक्के मिलते हैं, उनको कभी नहीं लेना चाहिए।
मुनक्के का क्वाथ कर के प्रायः द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट आदि बनाये जाते हैं। बहुत से आसवों में साबुत मुनक्का (बिना क्वाथ किये ही) डालने का भी निर्देश पढने को मिलता है, किन्तु इसको पका कर (क्वाथ बनाकर ही डालना चाहिए। कच्चा इस प्रधान द्रव्य और कच्चे स्वरस आदि से आसव अरिष्ट ठीक (सु स्वादु) नहीं बनते हैं। गिलोय, पुनर्नवा धत्तुर पंचांग, वासक, ब्राह्मी, शतावर आदि स्वरस अथवा इकच्चा डालकर बनाने से आसवारिष्ट खट्टे तैयार होते हैं तथा कभी-कभी इन सफेद कीड़े भी पड़ते नजर आते हैं।
अतः इनको सुखा कर ही काम में लेना उहए। घृत कुमारी रस का भी पकाकर ही काम में लाना चाहिए। पत्ते को छीलकर निकालने में थोड़े परिमाण में तो किसी भी प्रकार बनाया जा सकता है, फिर बड़ी दिक्कत होती है। और गूदा सहित सन्धान के लिए डाल दिया जाये तो सानने के बाद गूदा रूप में ही बहुत सा अंश निकल जाता है। अतः घृतकुमारी को पाकर टुकड़े-टुकड़े करके कड़ाही में दोगुने जल में डालकर पकाये और आधा जल झोष रहने पर उतारकर हाथों से मसलकर रस निकालकर काम में लेना चाहिए।
इस प्रकार रस का भी पाक हो जाता है और रस भी ठीक निकल जाता है। कुमारी आसव में लौह का मिश्रण किया जाता है, अतः लौह पात्र में उबालने में भी कोई हानि नहीं है। ऊपर तो मुनक्का व कच्चे रस वाली ओषधियों के विषय में हम लिख आये हैं, परन्तु अन्य और भी कोई अम्ल गुण विशिष्ट ओषधद्रव्य, जैसे-आंवला. कैध आदि यदि आसवा रिष्ट के क्वाथ द्रव्यों में हो तो उन्हें भी छोड़ देना चाहिए।
~ आसवो(Aasva) का स्वच्छ होना-
गुण-धर्म के अतिरिक्त आसवों का साफ-स्वच्छ होना भी अत्यावश्यक है। स्वच्छता निर्मलता हेतु आसवों का साफ और पुराना होना भी जरूरी है। नये आसवों को फिल्टर बैग, रि-फाइन करने की मशीन आदि से छानने के बाद कुछ दिन बोतलों के तलस्थ भाग में गाद बैठ जाती है और ऊपर स्वच्छ आसव दिखाई पड़ता है। आसवों का पुराना होना ही स्वच्छता के लिए आवश्यक है। आसव पुराना होने पर धीरे-धीरे गाद नीचे टंकियों में बैठ जाती है तथा स्वच्छ मद्यांशयुक्त भाग ऊपर रह जाता है, फिर उसको साधारण कपड़े से छान लेने पर आसव स्वच्छ गाद रहित पारदर्शक रहेगा।
~ आसवो (Aasva) की परीक्षा -
* आसवों के छानने के बाद बोतलों में भरकर कार्क लगाकर खूब हिलाने और कान के पास बोतल का मुँहह लगाकर कार्क खोलें। यदि आसव कच्चा होगा और उसमें कार्बन गैस अथवा एसिड उत्पन्न हो रहा होगा तो बोतल के मुँह से जोर की आवाज निकलेगी तथा बोतल फेन से भर जायेगी। कभी-कभी तो बोतल से बाहर आसव बहने लगता है। यदि दोष अधिक होगा तो बोतल हिलाने के बाद अपने आप कार्क उड़ जायेगा अथवा बोतल कमजोर रही तो फूट जायेगी।
अच्छी प्रकार बने आसवों में उपरोक्त बातें नहीं पायी जाती है। उनको बोतल में भरकर हिलाने के बाद कार्क खोलने से आवाज नहीं आती है एवं फेन/ झाग जल्द ही बैठ जाते है। कभी-कभी सूक्ष्म दोष रहने पर इस प्रकार की परीक्षा करके देखने पर भी स्पष्ट मालूम नहीं होता है| अतः बोतल मे आसव भरकर कार्क लगाकर धूप मे रख देना चाहिए| कुछ देर बाद उसकी उष्णता आने से अपने आप ही कार्क बाहर फेंक देगा| और कभी-कभी तो आसव बोतल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है|इस प्रकार के आसवो को काम मे नहीं लेना चाहिए|
जिस पात्र मे ऐसा आसव हो उसका मुख खोलकर दियासलाई जलाकर देखे , यदि आग बुझ जाए तो उसे 5-7 दिन मुख पर पतला कपड़ा बांधकर खुला रहने दे तथा प्रतिदिन देखते रहे, और यदि दियासलाई न बुझे तो उसे बन्द कर दें और 2-3 महीना पड़ा रहने के बाद काम में लें। यदि उसमें मधुरता कम हो तो ऊपर से उचित मीठा और मिला देना चाहिए। अच्छी प्रकार बने आसवारिष्ट मधुर व गुण युक्त होते हैं। इसके विपरीत कच्चे व अम्लता युक्त आसव सेवन करने से चित्त में उद्धिग्नता और बदन में लहर उत्पन्न होती है। ऐसे आसवों को व्यवहार में नहीं लेना चाहिए। गुणयुक्त आसव-अरिष्ट को सेवन करने से बदन में स्फूर्ति और चित्त में प्रसन्नता रहती है।
आसवों को बोतलों में भरते समय खूब सावधानी रखनी चाहिए। प्रायः आसवों को पात्र के लगे हुए नल से सीधे बोतलों में भरना चाहिए। बोतल में आसव भरते समय-बोतलों के मुँह पर महीन जाली या मोटा कपड़ा लगी हुई कूपी रख लेना चाहिए ताकि कोई दूषित वस्तु बोतल के भीतर न जा सके। पात्र के नल में फिल्टर बैग लटका देना चाहिए। यदि सीधे नल से भरने में सुविधा न हो या दूसरे स्थान पर ले जाकर भरना हो तो छोटे-छोटे पीतल या ताँबे के कलईदार बर्तन या एनामेल के कलईदार अथवा स्टेनलेस स्टील के बर्तन (जिसके मुख पर चूड़ीदार ढक्कन लगा हो उसमें) नल लगवा लें ,
और भरे हुए आसव के पात्र में फिल्टर बैग लगाकर इस प्रकार के बर्तन भर लें और भरने के बाद पात्र को ढांक कर किसी 1½-2 फुट ऊँचे स्थान पर रखकर, उसमें लगे नल द्वारा बोतलों को खूब धोकर व सुखाकर ही उसमें आसव भरें। यदि बोतल में कुछ पानी की बूँदे रहेगी तो कुछ दिन के बाद उसमें आसव विकृत होकर बोतल फूट जाने का भय रहता है तथा बोतलों को खूब लबालब नहीं भरना चाहिए यानी कुछ भाग खाली रखना चाहिए। अन्यथा आसवों में जोश आने से बोतलों के फूटने अथवा कार्क खुलने का भय रहता है।
~ आसवो का समान्य गुण-
* पाचन शक्ति को बढ़ाकर खाये गये पदार्थों को हजम करना, पेट में रुकी हुई वायु का अनुलोमन कर दस्त साफ लाना, शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न करना, मूत्र उचित मात्रा में तथा खुलकर त्याग होना और मूत्रवी विकृति दूर करना इत्यादि।
आसव-अरिष्ट यदि ठीक विधिपूर्वक बनाये गये हों तो वे कभी भी नहीं बिगड़ते हैं, बल्कि रखे रहने पर पुराने होकर और भी अधिक गुण युक्त हो जाते हैं। यह अनुभव तथा आयुर्वेद शास्त्रयुक्त सिद्ध बात है। आसव-अरिष्ट जितने अधिक पुराने होते हैं। उतने ही अधिक रुचिकर, स्वादिष्ट और तेज व शीघ्र गुणकारी होते हैं। (इसका कारण यह है कि-नये आसवों में ओषधियों की मिलावट से उत्पन्न होने वाले गुण भली प्रकार प्रकट नहीं हो पाते हैं। अतः लाभ कम होता है। पुराने आसवों में गुणों की निरन्तर वृद्धि होती रहती है।
पुराने आसवों व अरिष्टों में प्रायः तीक्ष्णता उत्पन्न हो जाती है। अतः आसवारिष्ट अकेला न लेकर बड़े (वयस्कों) या बच्चों को भी समान भाग पानी मिलाकर ही सेवन कराना चाहिए। बड़े व बलवान मनुष्यों को 2 से 8 तोला तक एवं कमजोर मनुष्यों को 1½ तोला तक तथा बच्चों को 3 माशा से 6 माशा तक और माता का दुग्धपान करने वाले शिशुओं को 15 से 30 बूँद आसवारिष्ट का सेवन करना-कराना चाहिए। आसवारिष्ट सेवन करते समय जल बराबर दोगुनी मात्रा में मिलाना चाहिए।
आसवारिष्ट को इस प्रकार से सेवन करना चाहिए कि ओषधि-मसूढ़ों में न लग कर गले से सीधे पेट में पहुँच जाये तथा जिस रोग-विकार/दोष के लिए आसवारिष्ट का सेवन किया जाये। उस रोग में बताये हुए पथ्यापथ्य/आहारा विहार का कठोरता के साथ सेवन करना अत्यावश्यक है। यदि स्वस्थावस्था में अपने स्वास्थ्य के रक्षार्थ आसवारिष्ट का सेवन किया जा रहा है, तो स्निग्ध (गाय-साधी-दूध आदि) एवं अन्य पौष्टिक पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आसवारिष्ट के प्रभाव से अन्न आदि शीघ्र ही पच जाते हैं।
